वित्तीय संपन्नता के बावजूद, समाज में सतत विकास की चुनौतियाँ बरकरार
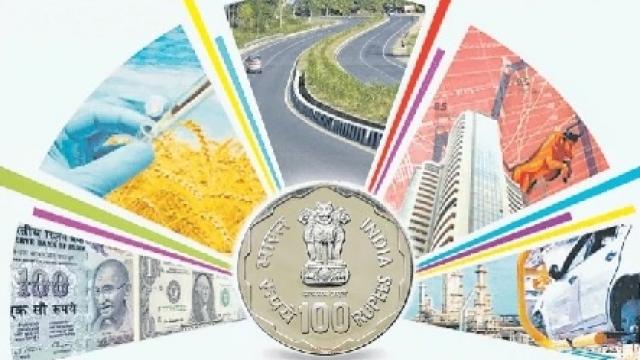
भारत ने सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में अच्छी प्रगति की है। विभिन्न देश संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास के लक्ष्यों की दिशा में जितनी अधिक उपलब्धि हासिल करते हैं, सूचकांक पर उनकी रैंकिंग उतनी ही बेहतर होती जाती है। भारत ने 2018 में इसमें 57 अंक मिले थे, जो 2023-24 में बढ़कर 71 हो गए। राज्यों ने भी कई लक्ष्यों में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेशों के कंपोजिट सूचकांक में 2020-21 और 2023-24 के बीच औसतन पांच यूनिट इजाफा हुआ है और कुछ ने तो आठ यूनिट तक वृद्धि की है। राज्य और जिला सूचकांक बनाकर एसडीजी का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर करने को जोर दिया जा रहा है, जिससे नीति निर्माण और सेवा आपूर्ति से जुड़ी संस्थाओं के बीच होड़ बढ़ गई है।
हरेक राज्य की प्रगति और उसके सामने आई चुनौतियों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि केरल और उत्तराखंड ने आठ-आठ लक्ष्यों में 80 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने छह-छह लक्ष्यों में 80 फीसदी से अधिक अंक लिए। मगर कुछ खास लक्ष्यों में कुछ राज्यों के अंक कम हुए हैं। 2 फीसदी से ज्यादा गिरावट देखें तो आंकड़े बताते हैं कि कुछ राज्यों में छह लक्ष्यों में अंक गिरे हैं। पंजाब और पश्चिम बंगाल ही ऐसे राज्य हैं, जो तमाम लक्ष्यों में लगातार प्रगति करते रहे। सभी लक्ष्य देखें तो लक्ष्य 1 (गरीबी समाप्त), लक्ष्य 5 (स्त्री-पुरुष असमानता), लक्ष्य 10 (असमानता में कमी) और लक्ष्य 16 (शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएं) पर प्रदर्शन फीका रहा। इनमें से से हरेक लक्ष्य के लिए 9 या अधिक राज्यों के अंक कम हुए हैं।
सतत विकास के लक्ष्यों पर केंद्र और राज्य सरकारों का जितना जोर है उसे देखकर माना जा सकता है कि दोनों सरकारें लक्ष्य हासिल करने के लिए बजट में काफी आवंटन कर रही होंगी। मगर सवाल है कि यह आवंटन काफी है या नहीं? खजाने में गुंजाइश कम होने के कारण कहीं प्रगति में रुकावट तो नहीं पड़ रही? विकासशील देशों में ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी संसाधनों का आकलन बताता है कि हर साल करीब 4 लाख करोड़ रुपये की दरकार है। कह सकते हैं कि भारत को और ज्यादा खर्च करना चाहिए। ज्यादा संसाधन हमेशा बेहतर होते हैं। मगर एक नजरिया और है। क्या खर्च हो रही रकम और अंकों में सुधार के बीच कोई संबंध हो सकता है?
कुछ राज्य इन लक्ष्यों के लिए तय बजट को अपने बजट दस्तावेज में शामिल कर रहे हैं। हरियाणा 2018-19 से ही ऐसे अनुमान पेश कर रहा है। ओडिशा और मेघालय ने भी बाद में यह शुरू कर दिया। ये दस्तावेज विभिन्न लक्ष्यों के लिए आवंटन और व्यय की सही तस्वीर दिखाते हैं। 2023-24 से पहले आवंटन या व्यय और इन लक्ष्यों पर हुई प्रगति की तुलना करने पर मिले-जुले नतीजे सामने आए। कुछ लक्ष्यों के लिए आवंटन बहुत हुआ मगर प्रगति नहीं हुई। उदाहरण के लिए लक्ष्य 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ओडिशा के परिणाम अच्छे नहीं रहे। असमानता कम करने वाले लक्ष्य 10 में भी उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। हरियाणा शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों वाले लक्ष्य 16 में और मेघालय गरीबी वाले लक्ष्य 1 और लक्ष्य 4 में पीछे रहा। तर्क दिया जा सकता है कि खर्च के नतीजे कुछ समय बाद सामने आ सकते हैं मगर यह अंकों में गिरावट की वजह तो नहीं हो सकती।
क्या खर्च और प्रगति की यह विसंगति प्रगति मापने में आ रही चुनौतियों के कारण है या दोबारा सोचना चाहिए कि हस्तक्षेप की योजना कैसे बनाएं और लागू करें? सावधिक या विश्वसनीय आंकड़े निगरानी परखने के लिए अहम हैं। प्रगति पर नजर रखने के लिए नियमित और विश्वसनीय आंकड़े जरूरी हैं। यह पता है कि सांख्यिकी की व्यवस्था सुधारी जा रही है, जिसके बाद बदलावों को अधिक प्रभावी ढंग से आंका जा सकता है। मगर अंकों में कमी को समझाने या खत्म करने के लिए शायद वे काफी नहीं होंगे।
सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़ी जानकारी बताती है कि लक्ष्यों के बीच तालमेल भी संभव है। क्या लक्ष्यों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? इन्हें समझने और इनका मॉडल तैयार करने से जनता के धन का सबसे अच्छा और भरपूर नतीजा मिल सकता है।

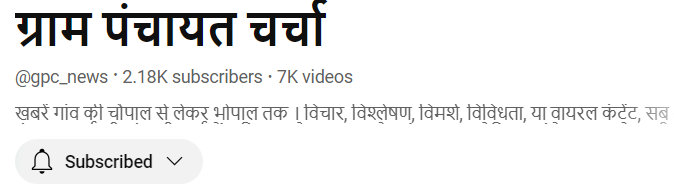




 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' में बिल्हा की मातृशक्ति का उल्लेख – छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति की स्वच्छता पहल को राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' में बिल्हा की मातृशक्ति का उल्लेख – छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति की स्वच्छता पहल को राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने की सौजन्य मुलाक़ात
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने की सौजन्य मुलाक़ात 24 घंटे में सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा.. बिहार के डिप्टी CM को धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अलर्ट
24 घंटे में सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा.. बिहार के डिप्टी CM को धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अलर्ट प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सरायपाली में 13 विकास कार्यों का किया लोकापर्ण एवं भूमिपूजन
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सरायपाली में 13 विकास कार्यों का किया लोकापर्ण एवं भूमिपूजन जब संगीत बना भक्ति का स्वर... इलैयाराजा की प्रस्तुति पर भावविभोर हुए प्रधानमंत्री मोदी
जब संगीत बना भक्ति का स्वर... इलैयाराजा की प्रस्तुति पर भावविभोर हुए प्रधानमंत्री मोदी हरिद्वार मनसा देवी भगदड़ हादसा, देवदूत बने एंबुलेंस चालक इरफान, बचाई कई लोगों की जान
हरिद्वार मनसा देवी भगदड़ हादसा, देवदूत बने एंबुलेंस चालक इरफान, बचाई कई लोगों की जान